MP कॉलेजों में डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू, प्रोफेसर्स के लिए नई चुनौती
मध्यप्रदेश (MP) में उच्च शिक्षा व्यवस्था में अब एक बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों के लिए डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही हर प्रोफेसर को प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे कॉलेज में उपस्थित रहना होगा। यह नियम राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों पर लागू होगा। यह बदलाव न सिर्फ शिक्षकों के कार्य संस्कृति को प्रभावित करेगा, बल्कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को भी नई दिशा देने का कार्य करेगा।
क्या है डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम?
डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम एक तकनीकी व्यवस्था है जिसमें कर्मचारियों की उपस्थिति को बायोमैट्रिक मशीन, मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। अब MP के कॉलेजों में प्रोफेसर्स को मोबाइल ऐप या बायोमैट्रिक डिवाइस के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि शिक्षक कॉलेज में समय पर उपस्थित हों और निर्धारित अवधि तक वहीं रुकें।
क्यों लिया गया यह फैसला?
राज्य सरकार ने यह फैसला उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने और प्रोफेसर्स की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से लिया है। लंबे समय से यह शिकायतें मिल रही थीं कि कई कॉलेजों में शिक्षक समय पर नहीं आते या फिर बिना बताए छुट्टी पर रहते हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है और संस्थान की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ता है।
डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम के माध्यम से इन समस्याओं पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। यह एक पारदर्शी और तकनीक-आधारित प्रणाली है जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के सही उपस्थिति का रिकॉर्ड तैयार करती है।
6 घंटे उपस्थिति क्यों जरूरी?
सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक प्रोफेसर को रोजाना कम से कम 6 घंटे कॉलेज परिसर में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षक सिर्फ कक्षा में लेक्चर देने तक ही सीमित न रहें, बल्कि छात्रों को अतिरिक्त मार्गदर्शन, प्रोजेक्ट वर्क, और अनुसंधान कार्यों में भी मदद करें।
इस कदम से कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी और छात्रों को ज्यादा समय तक शिक्षकों की उपलब्धता मिलेगी। साथ ही कॉलेज प्रशासन भी कार्य प्रबंधन में ज्यादा पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित कर सकेगा।
प्रोफेसर्स के लिए यह क्यों बनी चुनौती?
हालांकि यह निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है, लेकिन शिक्षकों के बीच इसे लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:
1. स्वतंत्रता में कटौती की आशंका
कुछ प्रोफेसर मानते हैं कि डिजिटल अटेंडेंस और समयबद्ध उपस्थिति से उनकी शैक्षणिक स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। रिसर्च और फील्ड वर्क करने वाले शिक्षकों के लिए कॉलेज में हर दिन 6 घंटे उपस्थित रहना व्यावहारिक नहीं होगा।
2. तकनीकी दिक्कतें
ग्रामीण और दूर-दराज़ क्षेत्रों में स्थित कॉलेजों में इंटरनेट और तकनीकी सुविधाएं उतनी सशक्त नहीं हैं। ऐसे में डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को लागू करना और सुचारु रूप से चलाना एक बड़ी चुनौती होगी।
3. मानव संसाधन की कमी
कुछ कॉलेजों में पहले से ही शिक्षकों की कमी है। अगर मौजूद शिक्षकों पर निगरानी बढ़ेगी और कार्य का दबाव अधिक होगा, तो इससे काम के बोझ में असंतुलन आ सकता है।
सरकार की ओर से क्या तैयारी?
मध्यप्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं:
-
डिजिटल अटेंडेंस के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल विकसित किए गए हैं।
-
कॉलेजों में बायोमैट्रिक मशीनें लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
-
शिक्षकों को नई व्यवस्था की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं।
-
जिन कॉलेजों में नेटवर्क या तकनीकी समस्या है, वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।
इसके अलावा, उच्च शिक्षा विभाग की ओर से मॉनिटरिंग सेल का भी गठन किया गया है, जो समय-समय पर उपस्थिति रिपोर्ट की निगरानी करेगी।
छात्रों और अभिभावकों की प्रतिक्रिया
इस फैसले को छात्रों और अभिभावकों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। उनका मानना है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और छात्रों को प्रोफेसरों से बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा।
छात्र क्या कहते हैं?
"पहले कई बार ऐसा होता था कि हमें क्लास कैंसल होने की जानकारी कॉलेज जाकर ही मिलती थी। अब जब प्रोफेसर्स की अटेंडेंस ट्रैक होगी, तो ये समस्याएं कम होंगी।"
— राहुल शर्मा, बी.एससी. छात्र, भोपाल
निष्कर्ष
डिजिटल अटेंडेंस और 6 घंटे की अनिवार्य उपस्थिति व्यवस्था से मध्यप्रदेश के कॉलेजों में अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इसके क्रियान्वयन में कुछ व्यवहारिक चुनौतियाँ हैं, लेकिन अगर इसे सही ढंग से लागू किया गया, तो यह शिक्षा प्रणाली के लिए एक सकारात्मक और दूरदर्शी कदम साबित हो सकता है।
सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों की चिंताओं को भी सुने और जहां जरूरी हो, वहां लचीलापन प्रदान करे। इस तरह यह पहल एक संतुलित और प्रभावी मॉडल बन सकती है, जिसे अन्य राज्यों में भी अपनाया जा सके।
अगर आप चाहें, तो मैं इस लेख को PDF या ब्लॉग पोस्ट फॉर्मेट में भी तैयार कर सकता हूँ। क्या आप इसे सोशल मीडिया या वेबसाइट पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं?

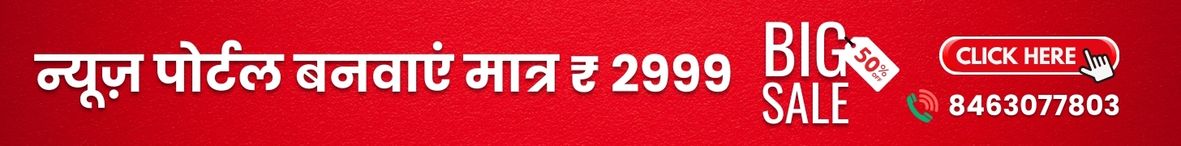

 TREND
TREND
.png)


.png)
.png)



.webp)

